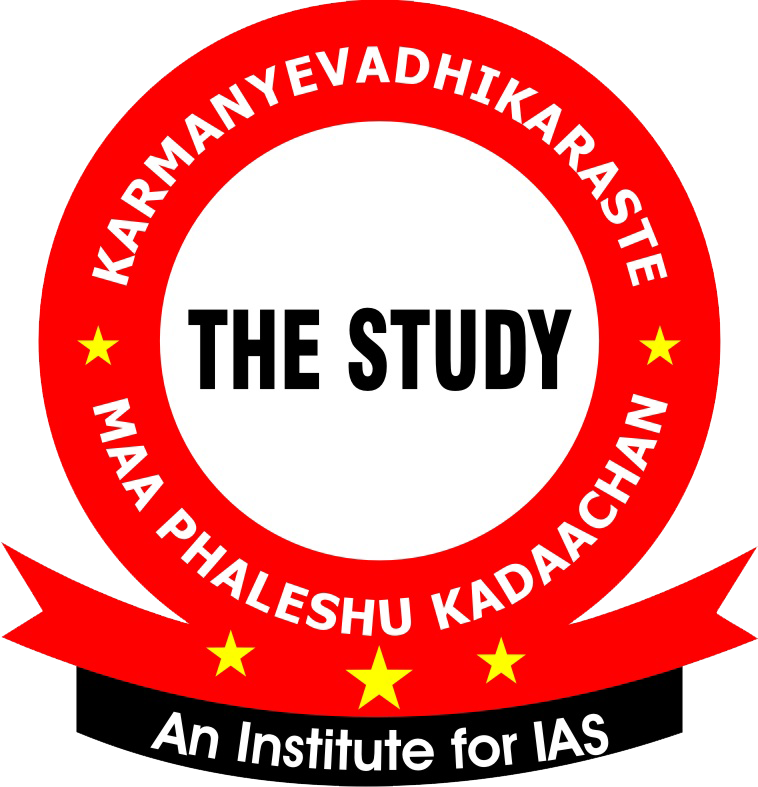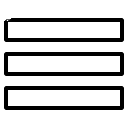Dec. 27, 2022
संवैधानिक चुप्पी, असंवैधानिक निष्क्रियता
प्रश्न पत्र- 2 (शासन एवं राज्य व्यवस्था )
स्रोत- द हिन्दू
चर्चा में क्यों ?
- राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित विधेयकों को दी गई स्वीकृति से संबंधित राज्यपाल की शक्तियों पर समय सीमा की अनिश्चितता के कारण राज्यपालों द्वारा उनके दुरुपयोग पर विचार-विमर्श किया गया।
पृष्ठभूमि
- 26 नवंबर, 1949 को जब संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाया गया था, तो भविष्य में संसद को लोगों की आकांक्षाओं और इच्छा के अनुसार संविधान को संशोधित करने की शक्ति प्रदान की गयी।
- संविधान का अनुच्छेद-200, राज्यपाल को राज्य विधानसभा द्वारा भेजे गए विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए समय-सीमा निर्धारित नहीं करता है। नतीजतन, कई विपक्षी शासित राज्यों के राज्यपालों ने लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों के जनादेश को भ्रमित करने के लिए इसका दुरुप्रयोग किया है।
संवैधानिक योजना
- अनुच्छेद - 200: यह एक राज्यपाल को कार्रवाई के चार विकल्प प्रदान करता है जब विधायिका द्वारा पारित विधेयक को उसकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल स्वीकृति तुरन्त दे सकता है , अनुमति रोक सकता है और विधेयक या विधेयक के किसी विशेष प्रावधान पर पुनर्विचार करने के अनुरोध के साथ विधेयक को विधानसभा को को लौटा सकता है।
- हालाँकि, यदि विधायिका राज्यपाल द्वारा सुझाए गए किसी भी संशोधन को स्वीकार या अस्वीकार किए बिना विधेयक को फिर से पारित कर देती है, तो वह संवैधानिक रूप से विधेयक को स्वीकृति देने के लिए बाध्य है।
- अनुच्छेद - 201 के तहत राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित भी रख सकते हैं।
विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए राज्यपाल को सशक्त बनाने के पीछे उद्देश्य:
- एक स्वतंत्र राज्यपाल केंद्र और राज्य बीच नियंत्रण और संतुलन के रूप में कार्य करेगा।
- यह जल्दबाजी में बनाए गए विधानों के खिलाफ एक सुरक्षा-वाल्व के रूप में कार्य कर सकता है और राज्यपाल की कार्रवाई से राज्य सरकार और विधानमंडल को इस पर पुनः नज़र डालने में सक्षम बनाता है।
हाल ही के विवाद:
- तमिलनाडु में, लगभग 20 विधेयकों को राज्यपाल की स्वीकृति का इंतजार है। राज्यपाल ने राष्ट्रीय पात्रता सह- प्रवेश परीक्षा से छूट के विधेयक को भी काफी विलंब के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा।
- इसी कारण तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल को हटाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा।
- केरल में, राज्यपाल ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह लोकायुक्त संशोधन विधेयक, 2022 और केरल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को स्वीकृति नहीं देंगे।
सुप्रीम कोर्ट
पुरुषोत्तमन नंबुदिरी बनाम केरल राज्य मामला (1962):
- एक संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि संविधान कोई समय सीमा नहीं लगाता है जिसके भीतर राज्यपाल को विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल द्वारा विधानमंडल द्वारा पारित कानून पर सहमति रोकना संविधान के संघीय ढांचे पर सीधे हमला करने जैसा है।
- विधेयकों को मंजूरी देने में देरी करना एक मनमाना कृत्य होगा, जो संविधान की भावना के खिलाफ है।
शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामला (1974):
- एक 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपनी औपचारिक संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग केवल कुछ प्रमुख अपवादों को छोड़कर अपने मंत्रियों की सलाह के अनुसार ही करेंगे।
नबाम रेबिया केस (2016):
- सुप्रीम कोर्ट ने बी. आर. अंबेडकर की टिप्पणियों का हवाला देते हुए कहा कि:
- संविधान के अनुसार, राज्यपाल के पास ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे वह अपने विवेक पर निष्पादित कर सकता/सकती है, लेकिन उसे कुछ कर्त्तव्यों का पालन करना होता है और सदन इस अंतर को ध्यान में रखना बुद्धिमानी होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संविधान का अनुच्छेद - 163 राज्यपाल को अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करने की सामान्य विवेकाधीन शक्ति नहीं देता है।
राजीव गांधी हत्याकांड (2018):
- सुप्रीम कोर्ट ने दो साल से अधिक समय से सात सजायाफ्ता कैदियों की रिहाई पर कार्रवाई करने में देरी पर राज्यपाल की विफलता का हवाला देते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की।
- संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCRWC) ने सुझाव दिया गया कि एक समय-सीमा होनी चाहिए।
- सरकारिया आयोग: विधेयक के प्रारूपण के स्तर पर ही राज्यपाल के साथ पूर्व परामर्श करके और इसके लिए समय-सीमा निर्धारित करके ,सहमति देने में राज्यपाल द्वारा की जाने वाली देरी से बचा जा सकता है।
- पुंछी समिति: राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल के महाभियोग के प्रावधान की मांग की गयी।
वैश्विक नियम
- यूनाइटेड किंगडम में, सम्राट के लिए संसद द्वारा पारित विधेयक को सहमति देने से इनकार करना असंवैधानिक है।
- ऑस्ट्रेलिया में, ताज द्वारा किसी विधेयक पर सहमति देने से इंकार करना संघीय व्यवस्था के लिए प्रतिकूल माना जाता है।
आगे की राह
- राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है। राज्य का नाममात्र प्रमुख होने के नाते उससे राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार उस शक्ति का प्रयोग करने की अपेक्षा की जाती है।
- कानून बनाने की प्रक्रिया में राज्यपाल की सहमति सबसे महत्वपूर्ण है और उसका कर्त्तव्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि एक निर्वाचित सरकार संविधान के मापदंडों के अनुसार काम कर रही है।
- यद्यपि किसी विधेयक की सामग्री के संबंध में असहमति हो सकती है, किन्तु उन्हें अपनी शक्तियों का उपयोग कानून को अरुचिकर बनाने के लिए नहीं करना चाहिए।
प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न
प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
- भारत के संविधान के अनुसार, राज्यपाल समय-समय पर सदन या राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर आहूत कर सकता है जिसे वह उचित समझे।
- राज्यपाल को हमेशा मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह पर कार्य करना पड़ता है और सदन के आह्वान पर वह स्वयं निर्णय नहीं ले सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- केवल 1 b. केवल 2 c. 1 और 2 दोनों d. न तो 1 और न ही 2
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न- “राज्यपाल का विवेकाधिकार मनमाना या काल्पनिक नहीं हो सकता है। ऐसे किसी भी अभ्यास के संदर्भ में अधिक ध्यान देने की जरूरत है।” टिप्पणी कीजिए।