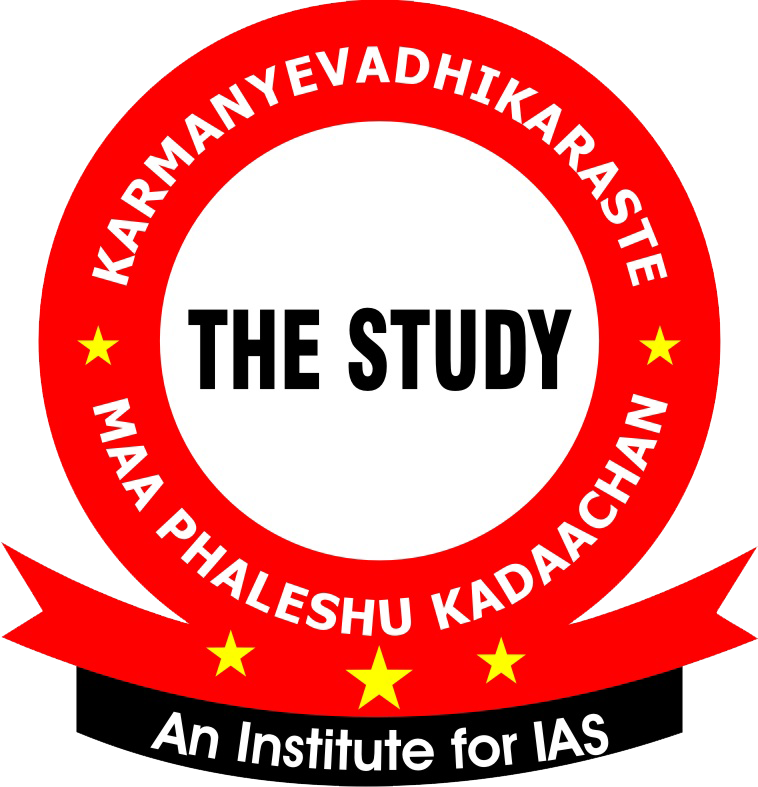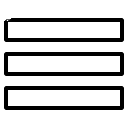29 december 2022
वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) जारी की।रिपोर्ट के अनुसार, सकल गैर-निष्पादित संपत्ति (GNPA) अनुपात 7 वर्षों में सबसे कम होने के साथ बैंकिंग प्रणाली की संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट क्या है?
वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट RBI द्वारा वर्ष में 2 बार जारी की जाती है।
यह देश में वित्तीय स्थिरता की स्थिति का विवरण देती है और इसे सभी वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के योगदान को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है।
FSR के हिस्से के रूप में, RBI एक प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण (SRS) भी आयोजित करता है, जिसमें यह विशेषज्ञों और बाजार सहभागियों से पाँच अलग-अलग प्रकार के जोखिमों - वैश्विक, वित्तीय, मैक्रोइकॉनॉमिक, संस्थागत, सामान्य पर वित्तीय प्रणाली का आकलन करने के लिए कहता है।
महत्व:
FSR बताती है कि अर्थव्यवस्था में बदलाव के लिए हमारी वित्तीय प्रणाली, विशेष रूप से हमारी बैंकिंग प्रणाली, कितनी मजबूत या कमजोर है।
साथ ही बताती है कि क्या और किस हद तक हमारे बैंक और अन्य ऋण देने वाली संस्थाएँ भविष्य के विकास का समर्थन करने में सक्षम होंगी।
उदाहरण के लिए, यदि FSR बताती है कि बैंकिंग प्रणाली में NPA या खराब ऋण का प्रतिशत अधिक है साथ ही यह भी दर्शाती है कि सरकार का राजकोषीय घाटा भी अधिक है, तो इसका मतलब है कि बैंक प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए न केवल संघर्ष करेंगे, बल्कि अगर बैंक लड़खड़ाते हैं तो सरकार के लिए उन्हें उबारना मुश्किल हो सकता है।
नवीनतम FSR से मुख्य निष्कर्ष:
सकल गैर-निष्पादित संपत्ति (GNPA)
नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA), बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए ऋण और बकाया राशि होती है, जिनके मूलधन और ब्याज में 90 दिनों से अधिक की देरी हो रही है।
रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर, 2022 में GNPA अनुपात घटकर 7 वर्षों में सबसे निचले स्तर 5 प्रतिशत पर आ गया है।
GNPA अनुपात का अनुमान मैक्रो-स्ट्रेस टेस्ट पर आधारित है, जो अप्रत्याशित घटनाओं के लिए बैंकों की बैलेंस शीट के लचीलेपन का आकलन करने के लिए किया जाता है।
पूंजी जोखिम (भारित) संपत्ति अनुपात (CRAR) -
CRAR एक बैंक की पूंजी का उसकी जोखिम-भारित संपत्ति और वर्तमान देनदारियों का अनुपात है।
बैंक का CAR जितनना अधिक होगा, वित्तीय मंदी या अन्य अप्रत्याशित नुकसान का सामना करने में उसके सक्षम होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी।
रिपोर्ट के अनुसार, 46 प्रमुख बैंकों का CRAR 15.8 प्रतिशत है जो न्यूनतम पूंजी आवश्यकता 9 प्रतिशत से कहीं अधिक है।
आक्रामक सीप प्रजाति
चर्चा में क्यों?
पुलिकट और एन्नोर के मछुआरों द्वारा सीपियों की एक आक्रामक प्रजाति के प्रसार पर चिंता व्यक्त की गयी है जो दोनों जलाशयों के झींगों के लिए खतरा रही है।
प्रमुख बिंदु
समुद्री जीवविज्ञानियों ने इन प्रजातियों की पहचान Mytella strigata या Charru सीपी के रूप में की है जो दक्षिण अमेरिका की मूल प्रजातियाँ हैं।
इन प्रजातियों ने केरल के वेम्बनाड सहित दुनिया के कई हिस्सों में ज्वारीय आर्द्रभूमि पर आक्रमण किया है। कट्टुपल्ली के बंदरगाहों पर जाने वाले जहाजों से गिट्टी के पानी के निर्वहन के कारण यह फैल रहा है।
आर्द्रभूमि में मानवीय हस्तक्षेप, प्रदूषण और प्रकृति के कार्यों ने प्रजातियों के तेजी से प्रसार को गति दी है।
खतरे: ये सीपियां नदी की तलहटी में कालीन की तरह फैल जाती हैं और इस प्रकार झींगों को भोजन या उन्हें तलछट में छिपने से रोकती हैं।
भारत में राज्यों के बीच विवाद समाधान
चर्चा में क्यों?
महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद गहराता जा रहा है।हाल ही में, महाराष्ट्र विधानसभा के दोनों सदनों ने विवाद को सुलझाने के लिए कानूनी रूप से समर्थन करने के लिए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया।
महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमा विवाद
महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद की उत्पत्ति राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के दौरान हुई थी।
1 नवंबर, 1956 से प्रभावी हुए इस अधिनियम ने राज्यों को भाषायी आधार पर विभाजित कर दिया।
1 मई, 1960 को अपने निर्माण के बाद से, महाराष्ट्र ने दावा किया है कि बेलागवी (तब बेलगाम), कारवार और निपानी सहित 865 गांवों को महाराष्ट्र में विलय कर दिया जाना चाहिए।
महाराष्ट्र का दावा है कि ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ मराठी प्रमुख भाषा है और इन्हें महाराष्ट्र में रहना चाहिए। हालाँकि, कर्नाटक ने अपना क्षेत्र छोड़ने से इनकार कर दिया है।
महाजन आयोग:
अक्टूबर, 1966 में, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मेहर चंद महाजन की अध्यक्षता में महाजन आयोग का गठन किया।
बेलगावी (तब बेलगाम) पर महाराष्ट्र के दावे को खारिज करते हुए, आयोग ने जाट, अक्कलकोट और सोलापुर सहित 247 गांवों/स्थानों को कर्नाटक का हिस्सा बनाने की सिफारिश की।
हालाँकि, आयोग की रिपोर्ट को महाराष्ट्र द्वारा सिरे से खारिज कर दिया गया था और 2004 मेंइसने फिर सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया।
विवाद निपटान
एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में केंद्र
अंतर-राज्यीय विवादों को अक्सर दोनों पक्षों के सहयोग से हल करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार एक सूत्रधार या तटस्थ मध्यस्थ के रूप में काम करती है।
उदाहरण के लिए, 1968 का बिहार-उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम और 1979 का हरियाणा-उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम इसी तरह लाया गया था।
न्यायिक निवारण
सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल अधिकार क्षेत्र में राज्यों के बीच विवादों का फैसला करता है।
संविधान का अनुच्छेद 131सुप्रीम कोर्ट को निम्नलिखितकिसी भी विवाद की स्थिति में मूल अधिकार क्षेत्र की अनुमति देता है:
- भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद ; या
- भारत सरकार और एक तरफ किसी राज्य या राज्यों के बीच और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद ; या
- दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद।
अंतर्राज्यीय परिषद
संविधान का अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को राज्यों के बीच विवादों के समाधान के लिए अंतर-राज्यीय परिषद गठित करने की शक्ति देता है।
परिषद की परिकल्पना राज्यों और केंद्र के बीच चर्चा के लिए एक मंच के रूप में की गई है।
1988 में, सरकारिया आयोग ने सुझाव दिया कि परिषद को एक स्थायी निकाय के रूप में अस्तित्व में रहना चाहिए और 1990 में यह एक राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से अस्तित्व में आयी।
2021 में, केंद्र ने अंतर-राज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया और निकाय में अब 10 केंद्रीय मंत्री स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में हैं।
भारत में सड़क दुर्घटनाएं
चर्चा में क्यों?
हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, पूरे भारत में दुर्घटनाओं में मारे गए प्रत्येक 10 में से 8 की मृत्यु सीट बेल्ट नहीं लगाने के कारण हुई।
भारत में सड़क दुर्घटनाएं- 2021 रिपोर्ट:
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वार्षिक रिपोर्ट 'भारत में सड़क दुर्घटनाएं - 2021' प्रकाशित की गई।
उद्देश्य- भारत में सड़क दुर्घटनाओं का गहन विश्लेषण और अवलोकन प्रस्तुत करना।
रिपोर्ट कैलेंडर वर्ष 2021 के दौरान देश में सड़क दुर्घटनाओं के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्रदान करती है।
यह रिपोर्ट कैलेंडर वर्ष के आधार पर एकत्र किए गए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभागों से प्राप्त आंकड़ों/सूचनाओं पर आधारित है।
विशेषताएं:
रिपोर्ट के अनुसार, 2021 के दौरान 4.12 लाख दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिसमें 1,53,972 लोगों की जान गई।
2021 के दौरान पीड़ितों में 18-45 वर्ष के युवा वयस्कों की संख्या 67.6% थी।
दुर्घटनाओं से जुड़े प्रमुख संकेतकों ने 2019 की तुलना में 2021 में बेहतर प्रदर्शन किया है।
हालांकि, 2019 में इसी अवधि की तुलना में 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में 1.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
राज्यवार आंकड़े-
उत्तर प्रदेश में 13.8% सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु का सबसे बड़ा भाग है, इसके बाद तमिलनाडु (10%), महाराष्ट्र (8.8%), मध्य प्रदेश (7.8%), और राजस्थान (6.5%) का स्थान है।
तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 2019 की तुलना में मृत्यु दर में वृद्धि देखी गई है।
उत्तर प्रदेश में सीटबेल्ट न लगाने के कारण कार सवारों की सबसे अधिक मौतें हुई हैं।