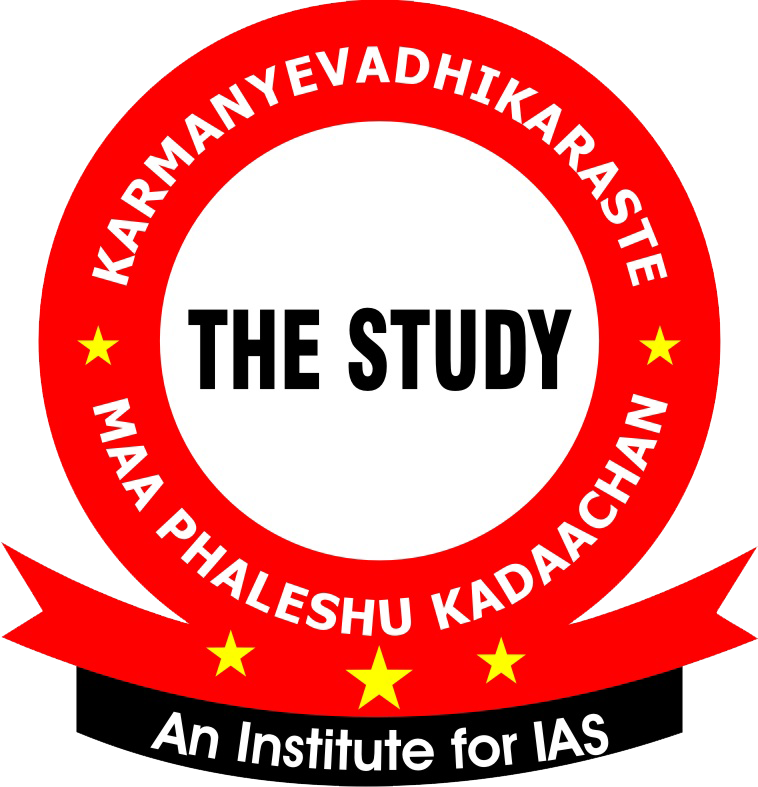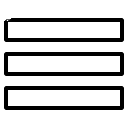Dec. 23, 2022
22 december 2022
डोकरा धातु शिल्प
चर्चा में क्यों?
- लाल बाजार (झारखंड की सीमा पर स्थित) डोकरा धातु शिल्प का केंद्र बनता जा रहा है।
प्रमुख बिंदु
- ढोकरा झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना जैसे राज्यों में रहने वाले ओझा धातु कारीगरों द्वारा प्रचलित घंटी धातु शिल्प का एक रूप है।
- हालांकि, अलग-अलग राज्यों में इस कारीगर समुदाय की शैली और कारीगरी अलग-अलग है।
- ढोकरा या डोकरा, को बेल मेटल शिल्प के रूप में भी जाना जाता है।
- इसका प्रलेखित इतिहास लगभग 5,000 वर्ष पुराना है।
- डोकरा कला बनाना एक कठिन प्रक्रिया है। प्रत्येक मूर्ति को बनाने में लगभग एक माह का समय लगता है।
- डोकरा कलाकृतियाँ मुख्य रूप से पीतल से बनाई जाती हैं और अत्यधिक अनूठी होती हैं, जिसमें टुकड़ों में किसी भी प्रकार का जोड़ नहीं होता है। पूरी वस्तु की पूर्णतः दस्तकारी की जाती है।
- पारंपरिक डिजाइन प्रकृति में अत्यधिक सौंदर्यपरक और संग्रहकर्ता की प्रसन्नता के प्रतीक माने जाते हैं।
प्रक्रिया क्या है?
- इसमें कई प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिसके लिए अन्य कच्चे माल के अलावा सात से आठ प्रकार की मिट्टी (क्ले) की आवश्यकता होती है।
- डोकरा बनाने की विधि में धातुकर्म प्रक्रिया को द्रवी मोम तकनीक के साथ जोड़कर सम्पन्न किया जाता है।
- विशिष्ट रूप और सुंदरता की कलाकृतियां बनाने के लिए हस्तशिल्प को मोम तकनीक के साथ धातुकर्म कौशल के संयोजन के लिए जाना जाता है।
- द्रवी मोम विधि मूर्ति निर्माण का एक अलग रूप है जिसमें सांचे का उपयोग केवल एक बार किया जाता है और टूट जाता है, जो हस्तशिल्प बाजार में अपनी तरह की एक अनूठी मूर्ति बनाता है।
- लॉस्ट वैक्स कास्टिंग की दो प्रक्रियाएँ हैं।
- पहली है सॉलिड कास्टिंग, जो दक्षिण में अपनाई जाने वाली विधि है और दूसरी है हॉलो कास्टिंग, जो अन्य राज्यों में प्रचलित है।
स्रोत- द हिन्दू
अर्बन-20
चर्चा में क्यों?
- G-20 के तहत, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय अहमदाबाद में अर्बन-20 कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।
प्रमुख बिंदु
अर्बन-20 (U-20) शिखर सम्मेलन क्या है?
- यह 12 दिसंबर, 2017 को पेरिस में वन प्लैनेट शिखर सम्मेलन में शुरू की गई एक शहरीय कूटनीतिक पहल है।
- अर्बन-20 (U-20), G-20 देशों के शहरों को जलवायु परिवर्तन, सामाजिक समावेशन, स्थायी गतिशीलता और किफायती आवास सहित शहरी विकास के विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने और सामूहिक समाधान प्रस्तावित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- C-40 सिटीज़ और युनाइटेड सिटीज़ एंड लोकल गवर्नमेंट्स (UCLG) ने U-20 को चेयर सिटी के नेतृत्व में आयोजित किया, जो G-20 मेजबान देश के आधार पर वार्षिक रूप से बदलती रहती है।
- U-20 2023 चक्र की अध्यक्षता अहमदाबाद शहर द्वारा की जाएगी।
- अहमदाबाद अपने अद्वितीय शहरी विकास और जलवायु परिवर्तन की पहल और समृद्ध संस्कृति एवं विरासत को प्रतिभागियों के सामने प्रदर्शित करेगा।
स्रोत- पीआईबी
सरकारी विज्ञापन में सामग्री विनियमन समिति (CCRGA)
चर्चा में क्यों?
- हाल ही में दिल्ली के लेफ्टिनेंट-गवर्नर (L-G) विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को निर्देश दिया है कि वे सरकारी विज्ञापन में सामग्री विनियमन समिति (CCRGA) के 2016 के आदेश को लागू करें।
सरकारी विज्ञापन में सामग्री नियमन संबंधी समिति (CCRGA) के बारे में:
- यह तीन सदस्यीय निकाय है।
- मई, 2015 में कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के निर्देश पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2016 में इसका गठन किया गया था।
- इस निकाय की स्थापना सभी मीडिया प्लेटफार्मों में केंद्र और राज्य सरकार के विज्ञापनों की सामग्री को विनियमित करने के लिए की गई है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को अपने स्वयं के निकायों का गठन करने के लिए भी अनिवार्य किया था।
- जहाँ कुछ राज्यों ने सार्वजनिक विज्ञापन सामग्री को विनियमित करने के लिए समितियों का गठन किया है, वहीं कुछ राज्यों ने अपने विज्ञापनों की निगरानी के लिए CCRGA को अनुमति दी है।
- सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सरकारों द्वारा सार्वजनिक वित्त पोषित विज्ञापन के लिए दिशानिर्देशों का एक सेट भी जारी किया था।
- उल्लिखित कुछ दिशा-निर्देशों में शामिल हैं कि सरकारी विज्ञापनों को राजनीतिक तटस्थता बनाए रखनी चाहिए और राजनीतिक हस्तियों के महिमामंडन या सत्ता में पार्टी की सकारात्मक छवि या सरकार की आलोचना करने वाली पार्टियों की नकारात्मक छवि पेश करने से बचना चाहिए।
- उनका उपयोग मीडिया घरानों को संरक्षण देने के लिए भी नहीं किया जाना चाहिए।
स्रोत- द हिन्दू
पाम-लीफ पाण्डुलिपि संग्रहालय
चर्चा में क्यों?
- केरल के मुख्यमंत्री तिरुवनंतपुरम के किले में पुनर्निर्मित केंद्रीय अभिलेखागार में आधुनिक ऑडियो-विजुअल तकनीक के साथ एक ताड़-पत्र पांडुलिपि संग्रहालय का उद्घाटन किया।
प्रमुख बिंदु
- यह अभिलेखागार विभाग, केरल सरकार द्वारा स्थापित किया गया था।
- 3 करोड़ रू. के इस संग्रहालय में आठ थीम-आधारित गैलरियां हैं जहाँ देश के सबसे बड़े ताड़ के पत्तों के संग्रह में से चुनिंदा पांडुलिपियों को प्रदर्शित किया जाएगा।
- एर्नाकुलम और कोझिकोड में केंद्रीय अभिलेखागार और विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में संग्रहीत 187 पुरानी और दुर्लभ पांडुलिपियों को इस संग्रहालय में रखा जाएगा।
- संग्रहालय में प्राचीन लिपियों; जैसे- वत्तेझुथु, कोलेझुथु, मलयम्मा और प्राचीन तमिल एवं मलयालम में पांडुलिपियां मौजूद हैं।
- पाण्डुलिपियाँ तत्कालीन त्रावणकोर, कोच्चि और मालाबार में कर, प्रशासन, और व्यापार से लेकर शिक्षा, जेलों जैसे विविध पहलुओं में इतिहास की एक आकर्षक झलक प्रदान करती हैं जो आम आदमी के लिए शायद ही सुलभ हो।
- इस संग्रहालय में में ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों के अलावा, स्क्रॉल, बांस की पट्टियां, और ताम्रपत्र शामिल हैं।
गैलरी:
- पहली गैलरी 'लेखन का इतिहास' विशेष रूप से केरल में लेखन के विकास का एक परिचय है जो आगंतुकों को मरयूर गुफा चित्रों तथा उत्कीर्णन और हड़प्पा में उपयोग किए गए स्टाम्प्स और मुहरों से उनकी प्रतिकृतियों के माध्यम से परिचित कराता है।
- मथिलाकोम अभिलेखों (श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में 3,000 कैडजन पांडुलिपि रोल का संग्रह) के बीच अन्य गैलरियां हैं -'भूमि और लोग', 'प्रशासन', 'युद्ध और शांति', 'शिक्षा और स्वास्थ्य', 'अर्थव्यवस्था', 'कला और संस्कृति'।
स्रोत- द हिन्दू
इको-सेंसिटिव जोन
चर्चा में क्यों?
- हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री ने राज्य में 115 घनी आबादी वाली पंचायतों में फैले संरक्षित जंगलों के छोर पर रहने वाले लोगों को आश्वासन दिया कि वे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ESZ) के आस-पास सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुझाए गए एक किलोमीटर के बफर जोन में अपनी जमीन या आजीविका से वंचित नहीं किए जायेंगे।
इको-सेंसिटिव जोन के बारे में:
- केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-2016) के अनुसार, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों की सीमाओं के 10 किमी. के भीतर भूमि को इको-फ्रेजाइल जोन या इको-सेंसिटिव जोन (ESZ) के रूप में अधिसूचित किया जाता है।
- जबकि 10 किलोमीटर के नियम को एक सामान्य सिद्धांत के रूप में लागू किया गया है, लेकिन इसकी सीमा अलग-अलग हो सकती है।
- केंद्र सरकार द्वारा 10 किमी. से अधिक के क्षेत्रों को भी ESZ के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है, यदि उनमें पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण "संवेदनशील गलियारे" शामिल हों।
इको-सेंसिटिव जोन क्यों बनाए जाते हैं?
- पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 2011 में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, आस-पास होने वाली कुछ मानवीय गतिविधियों द्वारा "संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र" पर नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए तथा उसका संरक्षण करने के लिए इको-सेंसिटिव ज़ोन को "शॉक एब्जॉर्बर" के रूप में बनाया गया है।
- इन क्षेत्रों को उच्च सुरक्षा की आवश्यकता वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा की आवश्यकता वाले क्षेत्रों के संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करने के लिए बनाया गया है।
- वे आस-पास रहने वाले लोगों की दैनिक गतिविधियों में बाधा डालने के लिए नहीं हैं, बल्कि संरक्षित क्षेत्रों की रक्षा करने और "उनके आस-पास के वातावरण को परिष्कृत करने" के लिए बनाए गए हैं।
इको-सेंसिटिव ज़ोन (ESZ) में कौन सी गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं?
- पेड़ों की कटाई जैसी विनियमित गतिविधियों के अलावा वाणिज्यिक खनन, आरा मिल, लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग आदि।
अनुमत गतिविधियाँ क्या हैं?
- प्रचलित कृषि या बागवानी पद्धतियां, वर्षा जल संचयन, जैविक खेती, आदि।
स्रोत- द हिन्दू