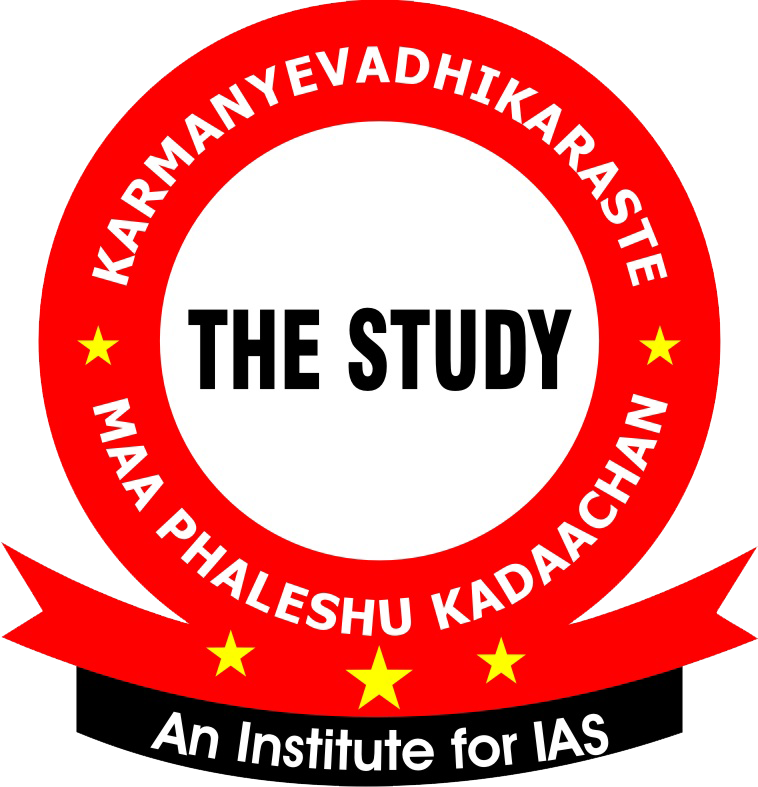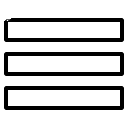बदलती राजनीति,असंगत राज्यपाल
प्रश्न पत्र- 2 (शासन एवं राजव्यवस्था)
स्रोत- द हिन्दू
चर्चा में क्यों ?
- राज्यपाल एक बार फिर से कई राज्यों में सार्वजनिक तमाशा बन रहे हैं, जैसा कि पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, झारखंड, दिल्ली और कुछ अन्य राज्यों में पहले भी देखा गया था।
प्रमुख बिंदु
- विचाराधीन राज्यों में चुनी हुई सरकारों के साथ उनकी समन्वयता में तीन मुद्दे सामने आते हैं।
बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के ऐतिहासिक फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 356 और इससे जुड़े विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की थी।
अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को इस फैसले के द्वारा रोक दिया गया। इस मामले के कारण केन्द्र-राज्य संबंधों पर भारी प्रभाव पड़ा।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 - केन्द्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की स्थिति में उस राज्य के राज्यपाल द्वारा सरकार को बर्खास्त कर, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है ।
- प्रथम- वे राज्य, जहाँ केंद्रीय सरकार के पक्षकार राज्यपाल और राज्य में दूसरे दल की सरकार उपस्थित हैं।
- द्वितीय- राज्यपालों के विरोधाभासी हस्तक्षेप संघ की कथित शक्तियों या संवैधानिक शुद्धता के नाम पर विरोध हैं।
- तीसरा- उनकी असहमति मीडिया के सामने खुलकर आने के कारण उनकी राजनीतिक विभाजन की रणनीति बल मिलता है।
- हाल ही में ऐसा देखने को मिला तमिलनाडु में, जहाँ के राज्यपाल आर.एन.रवि ने एक और मोर्चा खोल दिया है, यानी भारतीय राष्ट्रवाद के विचार को परिभाषित करना और तमिल लोगों को सबक देना।
- सौभाग्य से, राज्यों में केंद्रीकृत सरकार से इतर कुछ और राज्यपाल भी हैं, जिन्होंने अपनी-अपनी सरकारों के साथ मुद्दों को सुलझाने की दूरदर्शिता दिखाई है।
राज्यों में व्यापक परिवर्तन
- 1980 के दशक के उत्तरार्ध से, राज्यों की सापेक्ष स्वायत्तता के क्षेत्र में औपचारिक रूप से संवैधानिक ढाँचे में परिवर्तन किए बिना एक निर्णायक मोड़ आया।
- यह परिवर्तन नए राजनीतिक दलों के राज्यों पर ध्यान केंद्रित करने, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और राज्यों को आर्थिक जिम्मेदारी के अधिक हस्तांतरण के साथ उभरने में प्रकट हुआ था।
क्या राज्यपालों की नियुक्ति में मुख्यमंत्रियों की भूमिका होनी चाहिए?
- शक्ति और उत्तरदायित्व का यह परिवर्तन नीतिगत उपायों में भी परिलक्षित हुआ, जैसे- संविधान में 73वें और 74वें संशोधन द्वारा स्थानीय शासन को प्राधिकृत करना, शक्तियों का समावेश और हस्तांतरण पर बल दिया गया।
भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम,1992 - पंचायती संबंधों को मजबूत बनाना और उन्हें स्वायत अधिकार प्रदान करना है।
प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।
74वें संविधान (संशोधन) अधिनियम के तहत शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, जिसका उद्देश्य नगरों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना है।
- बेशक, राज्यों की सापेक्ष स्वायत्तता ने उनकी उपस्थिति के साथ-साथ जिम्मेदारियों को भी बढ़ाया है।
- राज्यों की यह बढ़ी हुई भूमिका किसी भी तरह से संघ की शक्तियों को चुनौती नहीं देती है, बल्कि आम तौर पर नई चुनौतियों और अवसरों का पूरक होती है।
राज्य का नेतृत्व
- भारत में दर्ज की गई राजनीति के कायापलट को देखते हुए, राज्य के नेतृत्व को सर्वोपरि रखा गया।
- प्रमुख के प्रदर्शन का असर न केवल संबंधित राज्यों पर, बल्कि पूरे देश पर पड़ता है। किसी राज्य-आधारित पहल का पड़ोसी राज्यों पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। अगर किसी क्षेत्रीय पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है तो केंद्र को कोशिश करनी चाहिए की वह उसे और बेहतर करे।
- दरअसल, राज्यपालों का यह मानना कि वे निर्वाचित राज्य नेतृत्व से अधिक बेहतर जानते हैं और वह व्यक्ति केंद्र में सत्तारूढ़ दल के हितों की सेवा भी नहीं कर सकता है, एक वास्तविकता के विरुद्ध है।
- भारत में राज्यपाल की संस्था के परिणामस्वरूप संवैधानिक तर्क आज भी मान्य हो सकते हैं, जो एक पुनर्भिविन्यास की मांग करता है।
- राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में, असंख्य सरोकार हैं,जैसे- राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, जो कि राज्य की सरकार के साथ राज्यपाल के संवाद का ढांचा तैयार करते हैं।
- बदले हुए संदर्भ में राज्य और अन्य जगहों पर संवैधानिक स्थिति पर जोर देने के बजाय जनता की आवाजों को सुनने और बारीकी से पालन करने की आवश्यकता है।
- इसके अलावा, अपने राज्य और केंद्र के बीच एक कड़ी के रूप में राज्यपाल, केंद्र के साथ-साथ बड़े पैमाने पर जनता के ध्यान में राज्य की व्यापक चिंताओं और वादों को लाता है, जिसे पक्षपातपूर्ण राजनीति दरकिनार कर सकती है।
- राज्यपालों को न केवल जमीन पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि अपने संस्थानों और सार्वजनिक संस्कृति में सामान्य अच्छे प्रकटन के अंतर्निहित विचार से भी अभ्यस्त होना चाहिए।