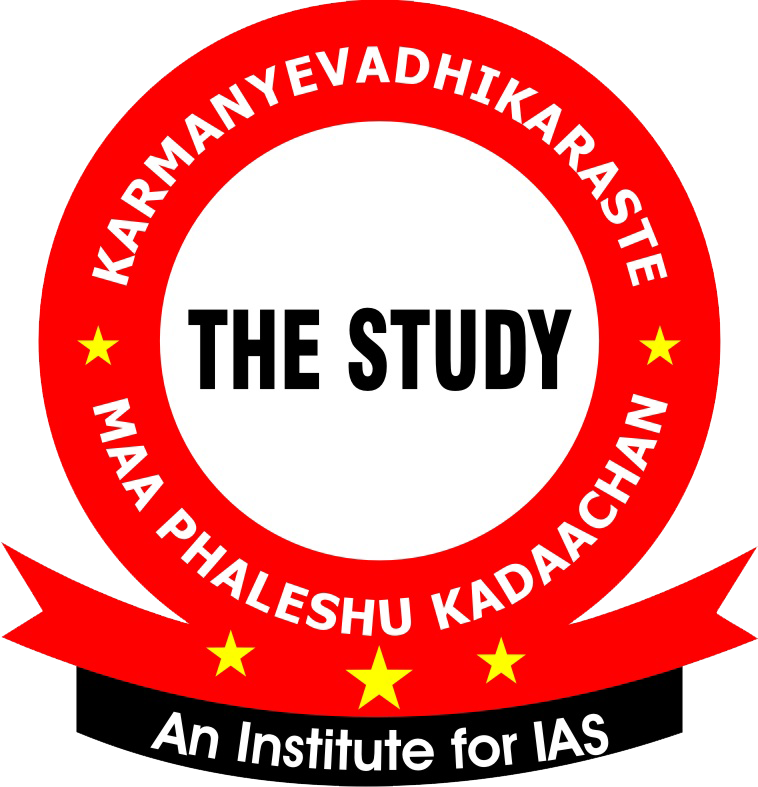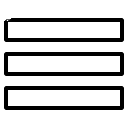कॉलेजियम प्रणाली पर विवाद
चर्चा में क्यों ?
न्यायिक नियुक्तियों की कॉलेजियम प्रणाली अपारदर्शी होने के कारण लगातार आलोचना का सामना कर रही है।
हाल ही में तेलंगाना, मद्रास और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में किए गए न्यायाधीशों के स्थानान्तरण ने विवादास्पद मुद्दों को जन्म दे दिया है। इसमें गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नाम भी शामिल था जिनके प्रस्तावित स्थानान्तरण का उस राज्य की बार काउंसिल द्वारा कड़ा विरोध किया गया था और न्यायधीश को स्वयं स्थानान्तरण से संबधित कोई सूचना प्राप्त नहीं थी।
हालिया सिफ़ारिशों में शामिल, अधिवक्ताओं को न्यायधीश बनाये जाने की सिफारिश को सरकार द्वारा ख़ारिज कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोबारा उन्हीं नामों की सिफारिश ने कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच विवाद को जन्म दिया।
संवैधानिक पृष्ठभूमि :
- अनुच्छेद 222: यह मुख्य न्यायाधीश सहित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति, CJI से परामर्श के बाद, एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं और स्थानांतरित न्यायाधीश को प्रतिपूरक भत्ता प्रदान किया जाता है।
- इस प्रकार सरकार किसी न्यायाधीश का तबादला कर सकती है, लेकिन केवल CJI से परामर्श करने के बाद।
- अनुच्छेद 143 – उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति की व्याख्या करता है अर्थात राष्ट्रपति को कानून या सार्वजनिक महत्व ,इन दो श्रेणियों के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है।
- भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत अधिवक्ताओं को अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जाता सकता है, न कि मुख्य न्यायधीश के रूप में।
कॉलेजियम प्रणाली क्या है?
- एस.पी. गुप्ता केस (1981) में, जिसे जज ट्रांसफर केस/फर्स्ट जज केस के रूप में भी जाना जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि CJI के साथ परामर्श का मतलब 'सहमति' नहीं, बल्कि विचारों का आदान-प्रदान है। इस प्रकार नियुक्तियों और स्थानांतरण के संबंध में कार्यपालिका को प्राथमिकता दी गयी।
- परन्तु इस स्थिति को सुप्रीम कोर्ट ने 'द्वितीय न्यायाधीश मामले' (1993) में खारिज कर दिया तथा कहा कि परामर्श का मतलब सहमति प्रकट करना है। इसमें वरिष्ठतम न्यायाधीशों के विचारों को ध्यान में रखकर बनाई गई CJI की राय को प्राथमिकता दी गयी। इसी तरह तीसरे न्यायाधीश मामले(1998 ) में सुप्रीम कोर्ट कहा कि परामर्श प्रक्रिया के तहत CJI एवं चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह ली जानी चाहिए। तभी से न्यायाधीशों की नियुक्तियां कॉलेजियम प्रणाली द्वारा की जा रही हैं।
- कॉलेजियम प्रणाली के तहत, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश (संख्या तीन से छह तक हो सकती है) तय करते हैं कि किसे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए।
99वाँ संविधान संशोधन क्या है?
- संसद द्वारा संविधान के 99वें संशोधन अधिनियम, 2014(न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम,2014) के तहत एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग(NJAC) का गठन किया गया।
- इस अधिनियम द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय (SC) के अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालयों (HC) के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबधित बनी कॉलेजियम प्रणाली को एक नये निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया।
- लेकिन वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि यह "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" अर्थात बुनियादी ढाँचे के सिद्धांतों के खिलाफ था क्योंकि इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति में राजनीतिक कार्यपालिका शामिल थी। परिणामतः पुरानी कॉलेजियम प्रणाली कार्यरत हो गयी।
स्थानातरण पर सुप्रीम कोर्ट की राय:
- SC ने इस विचार को खारिज कर दिया कि HC के न्यायाधीशों को केवल उनकी सहमति से स्थानांतरित किया जा सकता है क्योंकि स्थानांतरण शक्तियों का प्रयोग केवल जनहित में किया जा सकता है। इसके अलावा, राष्ट्रपति CJI से परामर्श करने के लिए बाध्य हैं।
स्थानातरण की आवश्यकता क्यों ?
- देश भर में प्रतिभाओं का आदान-प्रदान करने हेतु ।
- न्यायपालिका में स्थानीय समूहों के उद्भव को रोकने हेतु ।
- प्रत्येक उच्च न्यायालय के एक तिहाई सदस्यों में अन्य राज्यों के न्यायाधीशों को शामिल होना चाहिए।
स्थानान्तरण विवादास्पद क्यों ?
- इसे दंडात्मक तत्व के रूप में देखा जाता है।
- सुप्रीम कोर्ट के स्थानांतरण की प्रक्रिया अपारदर्शी है, इसके हस्तांतरण की शक्ति को हमेशा न्यायिक स्वतंत्रता के लिए एक संभावित खतरे के रूप में देखा गया है।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य
अतिरिक्त न्यायाधीश (Additional Judges)
- संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्त की जाती है।
- राष्ट्रपति,किसी योग्य व्यक्ति को उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकता है-
- यदि उच्च न्यायालय में अस्थायी रूप से कार्य का बोझ बढ़ गया हो।
- यदि उच्च न्यायालय में बकाया कार्य बहुत अधिक हो।
- अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की जाती है।
- किसी भी न्यायविद को 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जाएगा।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएँ- अनुच्छेद 124 [3]
- भारतीय संविधान के के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त मानदंडों की व्याख्या की गयी है :
- भारत का नागरिक होना चाहिए,
- कम से कम 5वर्षों के लिए एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या दो या दो से अधिक ऐसे न्यायालयों में उत्तराधिकार में रहा होना चाहिए,
- कम से कम 10वर्षों के लिए एक उच्च न्यायालय का या उत्तराधिकार में ऐसे दो या दो से अधिक न्यायालयों का अधिवक्ता रहा होना चाहिए,
- राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएँ- अनुच्छेद 217
- वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
- उसे भारत के क्षेत्र में 10 वर्षों के लिए एक न्यायिक रूप से कार्यरत होना चाहिए।
- उसे 10 वर्षों के लिए एक उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए।
संभावित प्रश्न
प्रश्न :निम्नलिखित में से किसे देश में किसी भी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने का अधिकार है?
(a) सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
(b) भारत के राष्ट्रपति
(c) संसद
(d) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की खंडपीठ
मुख्य परीक्षा प्रश्न
प्रश्न – कॉलेजियम प्रणाली की दक्षता को उसकी स्वतंत्रता और न्यायिक नियुक्तियों की पारदर्शिता के संदर्भ में समय-समय पर चुनौती दी गई है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)